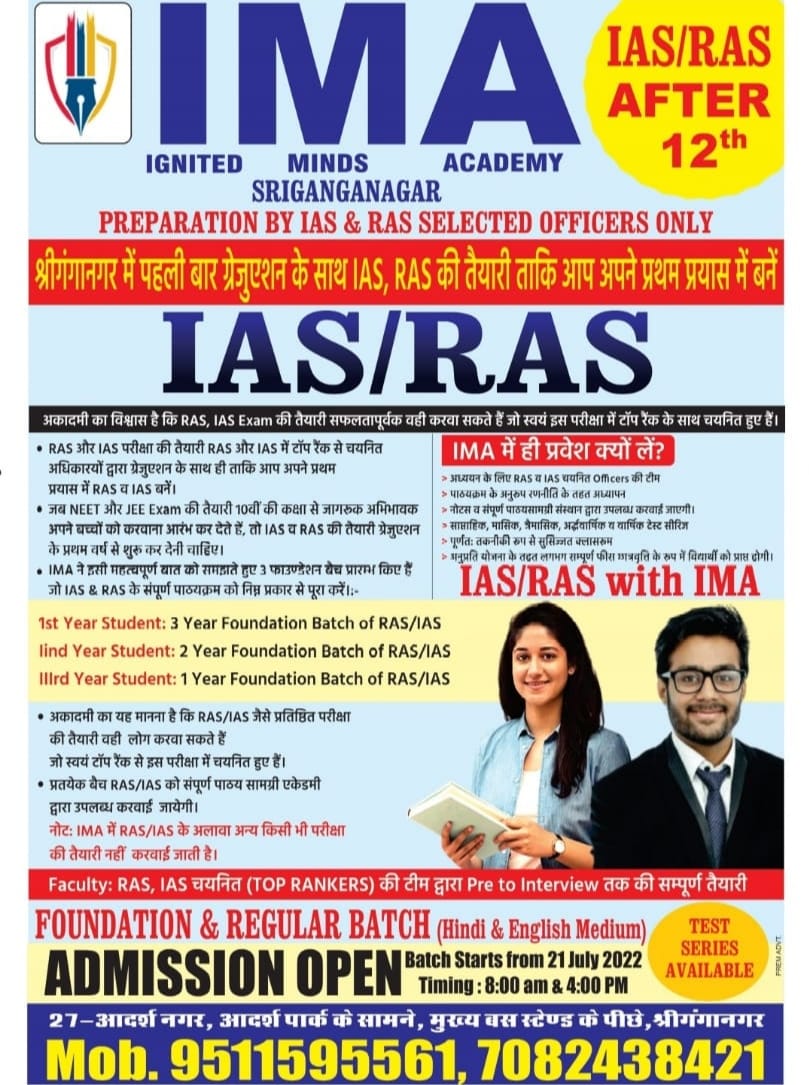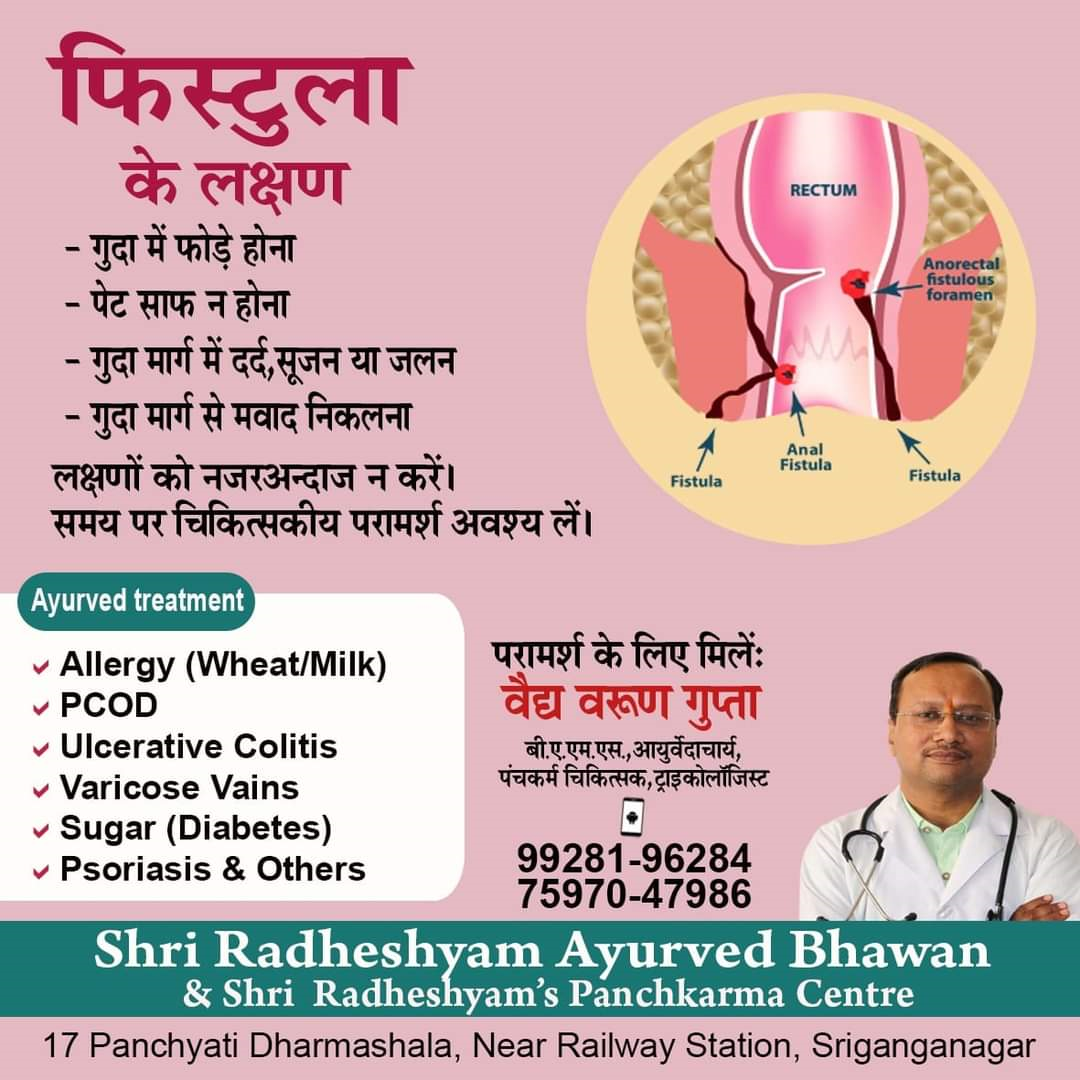संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. सरकार ने सत्र का प्रस्तावित एजेंडा पेश कर दिया है. इसमें कहा गया कि सत्र के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा में 75 सालों की संसद की यात्रा पर चर्चा होगी. बाकी के चार दिनों में चार विधेयकों पर चर्चा की जानी है. हालांकि, विपक्ष को लग रहा है कि सरकार कुछ बड़ा भी कर सकती है और वेन नेशन, वन इलेक्शन, देश का नाम सिर्फ भारत करने या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित भी कोई विधेयक पेश किया जा सकता है.

1947 से 2023 तक कई बार विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन शायद ही कभी यह इतना ज्यादा चर्चाओं में रहा होगा, जितना इस बार है. कब बुलाया जाता है विशेष सत्र, क्या विपक्ष की अनुमति भी जरूरी है, कब-कब बुलाया गया और इसकी प्रक्रिया क्या है? ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि विशेष सत्र क्या है, कब और कैसे बुलाया जाता है.
क्या होता है विशेष सत्र?
संविधान में कहीं भी ‘विशेष सत्र’ शब्द का जिक्र नहीं है. हालांकि, अनुच्छेद 352 (आपातकाल की उद्घोषणा) में ‘संसद की विशेष बैठक’ का जिक्र किया गया है. इस भाग को जोड़ने का मकसद देश में इमरजेंसी की घोषणा करने के सरकार की शक्ति को कंट्रोल करने के लिए किया गया था. इस प्रावधान के तहत अगर इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति को सदन की विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है. वहीं, लोकसभा के वन-टेंथ सांसद (यानी कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा) आपातकाल को अस्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति से विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं.
संविधान का अनुच्छेद 85(1) राष्ट्रपति को समय-समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं. राष्ट्रपति अपनी समझ के हिसाब से सत्र के लिए समय और स्थान निर्धारित कर सकते हैं. संविधान में प्रावधान है कि संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. विशेष सत्र और सामान्य सत्र के नियम एक समान होते हैं. विशेष सत्र और बाकी के तीनों सत्र अनुच्छेद 85(1) के तहत ही बुलाए जाते हैं. सामान्यत: एक साल में लोकसभा के तीन सत्र होते हैं. पहला बजट सत्र होता है, जो फरवरी से मई महीने के दौरान चलता है. दूसरा मानसून सत्र होता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच चलता है और तीसरा शीतकालीन सत्र साल के आखिर में नवंबर से दिसंबर महीने के बीच आयोजित किया जाता है. सत्र बुलाने का अधिकार सरकार के पास होता है. संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी इसका फैसला करती है और फिर औपाचारिक रूप से राष्ट्रपति इसे मंजूरी देते हैं.

दोनों सदनों का सत्र बुलाने का अधिकार है
संसद के तीन सामान्य सत्रों के अलावा जरूरत पड़ने पर संसद का सत्र भी बुलाया जा सकता है. अगर किसी विशेष विषय पर सरकार को तत्काल संसद सत्र बुलाने की जरूरत महसूस होती है तो वह स्पेशल सेशन बुला सकती है. ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 85 (1) राष्ट्रपति को दोनों सदनों का सत्र बुलाने का अधिकार देता है.
विपक्ष से चर्चा करना जरूरी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सवाल किया था कि 18 सितंबर से बुलाए जा रहे विशेष सत्र के लिए विपक्ष से चर्चा क्यों नहीं की गई और बगैर चर्चा के ही इसकी घोषणा कर दी गई. इस पर संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही विशेष सत्र की घोषणा की गई. उन्होंने संसद सत्र बुलाए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए संसदीय कार्य संबंधी कैबिनेट कमेटी के अनुमदोन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सत्र बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि संसद सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से संसद सत्र और मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं की जाती है. सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक होती है, जिसमें संसद में उठने वाले मुद्दों और कामकाज पर चर्चा की जाती है.